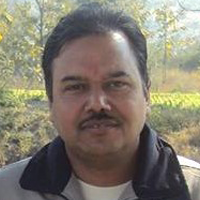“पुखराज हवा मे उड़ रए
हैं”- यह ग़ज़ल-संग्रह पिछले वर्ष प्रकाशित हुआ और ब्रज –ग़ज़ल को बाकायदा एक रह्गुज़र
मिली। ये रहगुज़र अब शाहराह बनने की राह पर है।मुल्के अदब की प्रेम-गली “ग़ज़ल” मे
यूँ भी बहुत भीड है रिवायती ग़ज़ल के ऐवानो और जदीद ग़ज़ल के अंगुश्त बदंदाँ कर देने
वाले शिल्पों /शाहकारों मे एक नया मकान एक नई तख़्ती कितने मक्बूल होंगे इसका फैसला
सौ मुंसिफों का मुंसिफ़ वक़्त ही करेगा !! लेकिन कमाल की बात ये है कि ऊपर वाले ने
नवीन सी चतुर्वेदी नाम की जो शय बनाई है इसके जोश ज़िद और जवानी के सामने ब्रज-ग़ज़ल
के भविष्य पर लगाये जाने वाले क़यास वसवसे की ज़द से निकल कर अब उमीदो एतबार की
पुख़्ता ज़मीन पर खडे नज़र आ रहे हैं।
हिन्दी को किसका ऋणी होना चाहिये ??!! आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
का !! बाबूश्याम सुन्दर दास का ?!! मेरे देखे तो हिन्दी को सबसे पहले भारतेन्दु और
देवकीनन्दन खत्री का ऋणी होना चाहिये क्योंकि जब भाषा का कोई विन्यास और मानदण्ड
बहुत सुष्पष्ट नहीं हो तो उसे रचना प्रक्रिया का अंग बनाना एक असुरक्षित रास्ता है
जिससे स्थापित साहित्यकार परहेज करते हैं –लेकिन जो शाहज़ादे इस चौथी सम्त जाते हैं
वो अपनी मिट्टी और नस्लों को बहुत कुछ ऐसा दे जाते हैं जिसका मूल्यांकन सिर्फ
आस्था , भावावेश और समर्पित धन्यवाद ही कर सकते हैं। बहुत सारी व्याकरणीय त्रुटियाँ
मिलेंगी दुष्यंत की ग़ज़ल में –लेकिन ये पहला और आखिरी नाम है जिसके नाम से हिन्दी
मे ग़ज़ल विधा की प्रतिष्ठा को मंसूब किया जायेगा। ब्रज –ग़ज़ल एक सोच है एक कोशिश है
एक आन्दोलन है एक तूफान है एक ग़ुबार है –मैं नहीं जानता –लेकिन शत प्रतिशत इसका
पूरा श्रेय नवीन नाम के मुश्ताको बेकरार को दिया जायेगा।
दोस्तो !! अगर औपचारिकता
की राह चलूँगा तो इस संकलन का सम्यक मूल्यँकन धुँधला पड जायेगा –ये मुझे किसी कीमत
पर मंज़ूर नहीं।लिहाजा “पुखराज हवा मे उड रए हैं” पर जो कहूँगा बेबाक कहूँगा। बकौल
इफ़्तिख़ार आरिफ –“मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है // सो मैं रहूँ न रहूँ इसको बार वर
कर दे” ऐसी ही शिद्दत के साथ नवीन ने ब्रज-ग़ज़ल को साहित्य मे स्थापित करने की जो
मुहिम छेडी है –उसके लिये इनकी जितनी प्रशंसा की जाय कम होगी। ये पुस्तक ब्रज –ग़ज़ल
की पहली पुस्तक है और ये नवीन सी चतुर्वेदी के लिये नहीं बल्कि गज़ल विधा में ब्रज
भाषा में कही गई गज़ल की स्थापना के लिये किया जाने वाला अभिनव प्रयास है !!
सवाल है कि हरियानवी ग़ज़ल
कही जा रही है, भोजपुरी ग़ज़ल कही जा रही है, लेकिन कोई बहुत बडी आवाजों मे ये प्रयास तब्दील नहीं
हो सके, इसका कारण क्या है ?! इस बिन्दु पर मैं कुछ देर तक इस बहस को रोकना चाहता हूँ !!
क्योंकि नवीन के संग्रह के अनेक शेर पढने के बाद ऐसा लगता है कि ब्रज –गज़ल युगों
से कही जा रही है !! हमे भाषा विज्ञानियों से इसका जवाब माँगना होगा !! हमे तारीख
मे इसका जो जवाब मिलता है वो ये है कि खडी बोली हिन्दुस्तानी अरबी फारसी बोलने
वाली फौज के भारतीय लोक भाषाओं के दीर्घकालीन संवाद और समागम की उपज है –अब अरबी
फारसी बोलने वाली फौज का पहला पडाव तो दिल्ली ही था और दिल्ली के निकट इलाकों पहली
और समृध भाषा कौन सी थी जिसने खडी बोली हिन्दुस्तानी के विकास में प्राथमिक भूमिका
निभाई होगी –ये ब्रज भाषा ही थी। सूरदास और रसखान द्वारा पूर्णत: परिपक्व और एक
बहुत बडे भौगोलिक क्षेत्र मे बोली जाने वाली भाषा। लिहाजा अगर ब्रज भाषा उर्दू के
अरकान पर खडी बहरों मे बहुत सुगमता से अपनी जगह बना ले तो कोई आश्चर्य नहीं । इस
फार्मेट मे किसी भी भाषा के लिये गुंजाइश है लेकिन पहले पहले सुनी गई नवीन की बज
–ग़ज़ल में एक ऐसी परिपक्वता नज़र आ रही है कि ब्रज गज़ल गज़ल विधा का नया आयाम लग ही
नहीं रही वरन वली दकनी के सृजन की भाँति ही गज़ल विधा का अभिन्न अंग जैसी लग रही
है।
नवीन ने अर्थ उद्बोधन के लिये ब्रज के समांतर
हिन्दी गज़ल भी कही है। इस संकलन का एक पोशीदा और दिलचस्प पहलू ये भी है कि गज़लकार
हिन्दी गज़ल मे महारत पहले से रखता है और ये भी कि अपनी अहर्निश प्रयोगधर्मिता और
नई रदीफ़ नये काफ़ियों के पैमाने पर इस संकलन का मूल्यांकन करने पर शाइर ने ब्रज
–भाषा की ग़ज़ल के अरूज़ को तवज़्ज़ेह दी है, गो कि इस शहादत की ज़रूरत नहीं थी।
नवीन चाहते तो अपना पहला हिन्दी गज़ल संकलन शान से प्रकाशित करवा सकते थे और अपना
चरचा करवा सकते थे –लेकिन इरादे पाक हैं और नीयत साफ है कि ये मुहिम ब्रज –ग़ज़ल की
स्थापना और विकास के लिये है।
मुझे इस संकलन में कई
शेर/ मिसरे इतने खूबसूरत मिले हैं कि उन्हें दोहों लोकोक्तियों और मुहावरों में
स्थान मिलना चाहिये –
पीर पराई और उपचार करें
अपनौ
संत –जनन के रोग अलग्गइ
होमुत एँ (1)
अपनी खुसी से थोरे ई सबने
करी सही
बोहरे ने दाब दूब के करवा
लई सही (2)
संग मे और जगमगामिंगे
मोतियन कूँ लडी में गूँथौ
जाय (3)
कहा जाता है कि किसी शायर
का कद अदब में जभी मुकम्मल होता है जब उसका चेहरा उसकी ग़ज़ल में दिखाई दे। तो जनाब
नवीन की ब्रज गज़ल का ठाठ ऐसा है कि इनकी गज़ल अधिकारी संवाद के धरातल पर खडी है। कई
ग़ज़लें मुसल्सल हैं और और अपनी वैचारिक समृद्धता के दम पर मुखातिब को सीधे अपने
इख़्तियार मे लेने की कुव्व्त रखती हैं। एक बात और कि ब्रज भाषा ग़ज़ल फार्मेट में और
खडी बोली हिन्दुस्तानी से अपनी निकटता के कारण इस विधा के माध्यम से फिर अपना
पुराना वैभव प्राप्त कर सकती है इसके बडे ही स्पष्ट इम्कान/संकेत इस संकलन मे
दिखाई पडे हैं।
हमारे गाम ही हम कूँ
सहेजत्वें साहब
सहर तो हमकूँ सपत्तौ ही
लील जामुत एँ (1)
न जानें चौं बौ औघड हमन
पै पिल पर्यो तो
कह्यो जैसे ई बासूँ
–सबेरौ ह्वै गयो ए (2)
नाच गाने के तईं पूजन हबन
मँहगे परे
आज के सस्ते समय मे आचरन
मँहगे परे (3)
बरफ के गोलन की बर्सा जब
हो रई ह्वै
ऐसे में हम अपना मूँड
मुडामें चौ (4)
सब्को इक दिन किनारे लगनो
हतै
और कुछ रोज बाढ मे बहि
ल्यौ (5)
किसी ग़ज़लकार के कैनवस का
सम्बन्ध उस परिवेश से भी होता है जो हमारे संस्कार और तर्बीयत का उत्तरदायी होता
है !! ब्रज –गोकुल –मथुरा –वृन्दावन एक भारतीय के मानस के अभिन्न अंग हैं चाहे
महाभारत के कारण चाहे भागवत्पुराण के कारण और चाहे गीता के कारण !! ये स्थान इस
देश के सर्वकालीन युगदृष्टा भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं और
हमारी समाजिक विचारधाराओं के समागम- स्ंक्रमण और प्रवाह का इन स्थानो से एक अटूट
सम्बन्ध है – चाहे वो धर्म की पुनर्स्थापना हो, चाहे वो रूढियों को तोड कर जीवन को
नये मानदण्डों पर स्थापित करने का सफल प्रयास हो, चाहे वो शुष्क़ और नीरस जीवन विहीन
जीवन की पैरवी करने वाली धर्मप्रणालियों मे नवीन संचेतना भर कर धर्म को जीवन
निर्माण और सामाजिक आरोह का सार्थक उपकरण बनाने का स्तुत्य प्रयास हो – ये सब कुछ
भारत के इसी भूखण्ड ब्रज मे सम्भव हुआ था और आज भी इस परिवर्तन का उपभोक्ता हमारा
समाज है। तो फिर अवश्य यहाँ की भाषा मे –उच्चारण मे – अभिव्यक्ति मे कुछ खास होगा
जिसने संवाद के सेतु को भावनाओं का पालना बना दिया। गौर कीजिये ब्रज भाषा की मिठास
को !!– क्या बात है इसमें!! –भले ही दग्ध वर्णों का इसमे इस्तेमाल हो लेकिन ब्रज
भाषा तो ह्रदय के लिये चाशनी से कम नहीं !! जिसने सुनी हो वही इस गूँगे के गुड का
स्वाद जानता है! दूसरी बात कि ग़ज़ल का एक अर्थ स्त्रियों से बातचीत भी है यानी आपको
नर्म, नाज़ुक, ह्रदयस्पर्शी और भावनाप्रधान होना होगा! इस मानदण्ड पर तो ब्रज सभी भाषाओ से
बाजी मार सकती है – ग़ज़ल के मर्क़ज़ के लिहाज से तो यही सबसे मुफ़ीद ज़बान होनी चाहिये।
इसलिये मुझे कौतुक नहीं है कि क्यों ब्रज –गज़ल अपने इब्तिदाई रूप मे ही इतनी मोहक
और आलोडित करने वाली प्रतीत हो रही है।
चन्द बदरन ने हमें ढाँक
दयौ
और का करते चन्द्रमा जो
हते (1)
आँख बारेन कूँ लाज आबुत ऐ
देख्त्वे ख्वाब जब नजर
बारे (2)
द्वै चिरिया बतराइ रई ऐं
चौरे मे
दरपन हमकूँ दिखाइ रई हैं
चौरे मे (3)
छान मारे जुगन जुगन के
ग्रंथ
इक पहेली ए दिल्रुबा कौ
रुख (4)
निश्चित रूप से ब्रज –गज़ल
के विचार को विचारधारा बनना चाहिये। इससे संवाद को एक निर्विवाद शैली मिलेगी जिसमे
प्रेम ही प्रेम छलकेगा- भाषा को एक आधार मिलेगा जिसमे भावना का प्राचुर्य होगा और
मंच को भी एक स्वर मिलेगा जिसमे सम्मोहन होगा। ये सब कुछ ब्रज गज़ल के विकास पर
निर्भर करेगा। ये दौरे हाज़िर की ज़रूरत भी है क्योंकि गज़ल के मंच को भी फिरकापरस्ती
की ऐशगाह बनाने की कोशिशे खुलेआम की जा रही हैं।
नवीन ने इस पुस्तक की
भूमिका में भी स्पष्ट किया है कि डाक्यूमेण्ट की गई ब्रज भाषा और मथुरा क्षेत्र
में बोली जाने वाली ब्रज भाषा मे भिन्नता के बावज़ूद समरसता है यानी दोनो स्थानो की
भाषा का इम्पैक्ट समान है – होनी भी चाहिये – वगर्ना लखनऊ की लिखी पढी जाने वाली
ज़ुबान बहुत ज़हीन है लेकिन चौक नख़्खास मे बोली जाने वाली ज़ुबान सुनने लायक भी नहीं
आज की तारीख़ मे।
जैसे ई पेटी में डार्यो बोट , कुछ ऐसो लग्यो देवतन ने
जैसें महिसासुर कूँ बेटी दै दई
इस शेर का मिसरा ए अव्वल
हमारी राजनैतिक विवशता का सम्पुट है तो मिस्रा ए सानी एक बेहतरीन तश्बीह है। लेकिन
इसके आगे देखिये ये शेर भाषा के साथ संस्कृति की भी पैरवी और परवरिश कर रहा है।
घर को रस्ता सूझत नाँय
हम सच में अन्धे ह्वै गये
बहुत सामान्य बात से एक
असाधारण पहलू निकाला है –हम अपने स्व के दायरे को भूल चुके है – अपस्ंस्कृति के
शिकार है मगरिबी तहज़ीब की ओर नई नस्लें माइल हैं और बकौल शुजा ख़ाबर –इन तेज़ उजलो
से बीनाई को खतरा है –तो हम आज इसके चलते अपने दिशाबोध और उद्देश्यों को भूल से
चुके हैं।
जबै हाथन में मेरे होतु ऎ
पतबार
तबै पाइन में लंगर होतु ऐ
भइया
जीवन के संसाधनो और
प्रवाह के साथ एक न एक मजबूरी –और क्या खूब पतबार और लंगर शब्दो का इस्तेमाल किया
है।
चैन से जीबो हू दुसबार
भयौ है अब तौ
दिल समर जाय तौ अरमान मचल
जामतु ऐं
दिल किसी तौर सम्भाला तो
जिगर बैठ गया - जैसी बात है इस शेर में।
हम तो कब सूँ सेहरा बाँधे
बैठे हतें
आज कहौ तो आज इ माँग भरें
साहब
हम हैं मुश्ताक और वो
बेजार
या इलाही ये माजरा क्या
है ??!!
हम उदासी के कोख जाये
हतें
जिन्दगी कूँ न रास आये हम
हम एक चीत्कार से जीवन
आरम्भ करते हैं और एक हिचकी पर हमारा जीवन समाप्त हो जाता है –ये हमारे युग की
-जीवन की विडम्बना है- जो कमोबेश हमारी नियति बन चुकी है।
नवीन के इस संकलन में
भाषा के वर्तमान स्वरूप –आम बोलचाल की भाषा इतने सहज्ग्राह्य रूप में इस्तेमाल की
गई है कि उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जो भाषा और व्याकरण की शुद्धि के केशवदास
हैं जिनके हिसाब से भाषा इतनी शुद्ध होनी चाहिये कि अस्पृश्य हो जाय – ये लोग
अरूज़े फिक्रो फन और मेयार के नाम पर अव्यवहारिक भाषा और नितांत पुस्तकीय
अभिव्यक्तियों के असीर होते हैं। ऐसों के उपालम्भ का बुरा मानने की ज़रूरत नहीं।
अगर रेगिस्तान को शस्य श्यामल करना है तो पहली बरसात को भाप बनना ही होगा।
इस संकलन में इरेज़र, इंवेस्ट,इस्माइल, मीटिंग , ट्राफी, बिल्दर डाक्टर , टैक्स एक्सपोर्ट जैसे
अंग्रेज़ी शब्दों को सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है – बिप्र छ्त्री
बनिया किरपा गोरस घुमेर जैसे ठेठ हिन्दी के शब्द मिजाज़ और माहौल बनाने में समर्थ
हैं इसके सिवा एक समर्थ ग़ज़लकार के पास जो काइअनाती मनाज़िर होते हैं और उनके
सिम्बल्स जिस भावना और विचार के सम्वाहक होते हैं उनका भी बहुत खूबसूरत प्रयोग इस
पुस्तक में मिलता है।
इस संकलन की हर ब्रज गज़ल
के समांतर हिन्दी ग़ज़ल भी शाइर ने कही है और कई शेर इतने शानदार हैं कि उनका ज़िक्र
न करना एक भूल होगी –
इतने रोज़ कहाँ थे तुम
आइने शीशे हो गये (1)
ये क्या कि रोज़ बहारों को
ढूँढते हैं हम
कभी –कभार खुद अपनी भी
जुस्तजू हो जाय (2)
कोई उस पार से आता है
तसव्वुर लेकर
हम यहाँ खुद को कलाकार
समझ लेते हैं (3)
(देनहार कौउ और है भेजत है
दिन रैन
लोग भरम हम पर धरै जाते
नीचे नैन ( रहीम))
ओस की बूँदें मेरे चारों
तरफ़ जमा हुईं
देखते देखते दरिया के
मुकाबिल हुआ मैं (4)
(मैं अकेला ही चला था
जानिबे मंज़िल मगर
लोग साथ आते गये और
कारवाँ बनता गया)
लडखडाहट पे हमारी कोई
तनक़ीद न कर
बोझ को ढोया भी है सिर्फ
उठाया ही नहीं (5)
माथुरस्थ माथुर् चतुर्वेद
संस्कार में जन्मे नवीन सी चतुर्वेदी आज की तारीख में मुम्बई शहर में बायोमीट्रिक
–सिम और सी सी टी वी व्यवसाय से जुडे हैं –यानी इस व्यक्ति ने ब्रज –गोकुल मथुरा
–व्रन्दावन गली हाट बाज़ार गाँव कस्बे की ज़िन्दगी को बहुत निकट से देखा है – हिन्दी
के सभी छ्न्दों ( कवित्त सवैया दोहा कुण्डली ) मे इन्हें महारथ हासिल है –गज़ल की
शाहराह पर भी कम समय में ये तेज़ कदम चल कर बहुत आगे पहुंचे हैं और आज मरीन ड्राइव
और नरीमन पाइंट वाले शहर में 1500 वर्ग फ़ीट के ऐसे घर में रहते हैं जिसके चारों ओर
सम्मोहित कर देने वाली हरियाली है। मुम्बई में अगर आपकी सुबह-शाम पक्षियों के कलरव
को सुन सकती है तो आप यकीनन भाग्यशाली हैं – ये घर नवीन का व्यक्तिगत चुनाव है ।
इस सफर और इस जीवन शैली का नाम नवीन है। कोई आश्चर्य नहीं कि जीवन के इस सफर की
सारी अनुगूँज उनकी ग़ज़लों मे मिलती है। ठेठ देशज शब्द – प्रचलित अंग्रेज़ी शब्द
–प्रांजल हिन्दी शब्द – गज़ल के रिवायती अल्फाज़ – हाट -बाज़ार -गली नुक्कड – मल्टी
स्टोरी – प्रयोग -परम्परा सभी कुछ नवीन की ग़ज़ल ने आत्मसात कर रखे हैं और इसके ही
साथ उन्होंने इस अनुभूति को बज भाषा और ग़ज़ल विधा के माध्यम से एक नई रहगुज़र पर
उतार दिया है। नवीन जदीदियत के दुस्साहस की हद तक पैरोकार हैं – अनेक बहुत अच्छे
शेर कहने के बाद भी वो सिर्फ उनपर आश्रित नहीं रहते वरन हमेशा प्रयोगधर्मिता को
तर्ज़ीह देते हैं। इसके सिवा आप नवीन के सोच को बदल नहीं सकते – नवीन मात्र वैचारिक
धरातल पर नहीं जीते वरन विचार को कर्मभूमि पर उतारने वाले हठयोगी भी हैं – बहुत कम
समय में ब्रज ग़ज़ल को आकशवाणी कार्यक्रमों में स्थान मिलने लगा है और टीवी
प्रोड्यूसरों ने इसके प्रसारण में रुचि दिखानी आरम्भ कर दी है – ये नवीन की ही
अहर्निश ऊर्जा का प्रतिफल है।
“ठाले- बैठे” ब्लाग में
उन्होने पुराने छन्दों पर अनेक सफल आयोजन किये और यह साबित किया कि अगर प्लेटफार्म
दिया जाय और कंवीनर समर्पित हो तो किसी भी विधा को आज भी पुनर्जीवित किया जा सकता
है और साहित्यकारों को उनके विभव से परिचित कराया जा सकता है। बज –ग़ज़ल एक नवीन
विचार है और ब्रज भाषा के माधुर्य और गज़ल की स्वीकार्य बहरों के अर्कान के साथ
इसका सहज समागम, मुम्किन है कि अभिव्यक्ति को एक नया संगीत और नया स्वर उपलब्ध करा दे।
भारत मे जब पश्चिमी संगीत के कदम बढे तो गुरुदास
मान –इला अरुण ने पंजाबी राजस्थानी नृत्य और संगीत का रैप म्यूज़िक के साथ एक
ब्लेण्ड प्रस्तुत किया था जो सुपर्हिट रहा। हमारी मिट्टी और चेतना की सिफत ऐसी है
कि अगर कोई साँसारिक व्रत्ति हमे निगलने के लिये आती है तो हम उसे आत्म्सात कर
लेते हैं। ग़ज़ल पर भी अर्से से अल्लामा सम्प्रदाय का कब्ज़ा है –ये लोग “लहर” को 21 के वज़्न में इस्तेमाल कर
सकते हैं “ब्राहमण” को बिरहमन उच्चारण करते हैं “धारा” को पुर्लिंग मे इसतेमाल
करते हैं –लेकिन देवनगरी ग़ज़ल के शाइरों की तंज़ो मलामत में कहीं चूक नहीं करते ताकि
इस विधा पर उनका एकाधिकार बना रहे। जबकि ग़ज़ल एक विधा के रूप में खाँटी उर्दू की
असीरी में रह ही नहीं सकती। जब इस विधा के पास इतना विशाल पाठक वर्ग है तो इस नदी की अन्य
धारायें भी बहेंगी और उनमे से कोई अपने प्रवाह और लहरों के बल पर एक अलग पहचान
बनाने में निश्चित रूप से सफल भी हो सकती है। ब्रज भाषा में ये अनासिर बडे साफ
दिखाई दे रहे हैं।
मुझे अपने भाई नवीन के जोश ज़िद और
जवानी पर गर्व है –इनकी सतत और अहर्निश ऊर्जा पर गर्व है –इनकी एकला चलो रे – never say die spirit पर गर्व है और इन्होने अनेक बार साबित किया है कि Impossible is a word in the the dictionary of fools . मेरी असीमित शुभ्रकामनायें इनके साथ
हैं। मैं भी आने वाले दिनो में उस लम्हे का शाहिद बनना चाह्ता हूँ कि अपने बच्चों
से कहूँ कि – ये जो ब्रज –ग़ज़ल आज टेक्ट बुक्स मे पढाई जा रही है इसका आरम्भ
तुम्हारे चाचा नवीन ने किया था।
माँ सरस्वती तुम पर हमेशा
ऐसी ही वरदहस्त रहें नवीन !!–सदा सुखी रहो ।
मयंक अवस्थी (8765213905)